भारत-अमेरिका समुद्री साझेदारी: दूरियों से भरोसे तक का सफर
दिसंबर 1991 में शीत युद्ध बिना किसी गोलीबारी के समाप्त हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया और अमेरिका अकेला महाशक्ति बनकर उभरा।
 सी. उदय भास्कर (सेवानिवृत्त कमोडोर, नौसेना विश्लेषक) / image provided
सी. उदय भास्कर (सेवानिवृत्त कमोडोर, नौसेना विश्लेषक) / image provided
शीत युद्ध के दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते को अक्सर ‘अलग-थलग पड़ी दो लोकतंत्रों’ के रूप में जाना जाता था। यह वही शीर्षक है जो अमेरिकी राजनयिक डेनिस कक्स की प्रसिद्ध पुस्तक का भी विषय बना। यह विडंबना थी कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और रणनीतिक दृष्टिकोण के अंतर के कारण एक-दूसरे से दूर थे। इस दूरी का सबसे बड़ा कारण था — परमाणु नीति पर असहमति, क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
शीत युद्ध के बाद नई शुरुआत
दिसंबर 1991 में शीत युद्ध बिना किसी गोलीबारी के समाप्त हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया और अमेरिका अकेला महाशक्ति बनकर उभरा। इसी वर्ष भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग की औपचारिक शुरुआत हुई, जब लेफ्टिनेंट जनरल क्लॉड एम. किकलाईटर की पहल पर 'किकलाईटर प्रस्ताव' तैयार किया गया। इसका उद्देश्य था भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंधों को धीरे-धीरे विकसित करना।
यह भी पढ़ें- भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी: समुद्री सहयोग का नया अध्याय
तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने बदले हुए अंतरराष्ट्रीय माहौल को भांपते हुए अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग के लिए सावधानीपूर्वक संवाद शुरू किया। शुरुआत में संयुक्त अभ्यास, स्टाफ एक्सचेंज और रक्षा परामर्श जैसे कदम उठाए गए ताकि विश्वास की खाई को पाटा जा सके।
MALABAR अभ्यास से सहयोग की लहर
सबसे पहले भारतीय नौसेना ने इस अवसर को समझा। मई 1992 में पहला भारत-अमेरिका नौसैनिक अभ्यास 'मालाबार' (MALABAR) आयोजित हुआ। उस समय ये अभ्यास सीमित दायरे में थे— बुनियादी नौसैनिक चालें, संचार अभ्यास और खोज-बचाव ऑपरेशन। धीरे-धीरे मालाबार का स्वरूप विस्तृत होता गया। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए— जो बाद में क्वाड (Quad) समूह के चार सदस्य देशों के रूप में उभरे।
9/11 के बाद नया विश्वास
11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका की सैन्य तैनाती हिंद महासागर तक पहुंची। इस दौरान भारतीय नौसेना ने अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को मलक्का जलडमरूमध्य तक एस्कॉर्ट किया, ताकि अमेरिकी युद्धपोत अन्य अभियानों में लग सकें। यह कदम भारत को एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता (Security Provider) के रूप में स्थापित करने वाला साबित हुआ। यही वह दौर था जब भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी ने व्यावहारिक रूप लेना शुरू किया।
परमाणु समझौते से रिश्तों में नई दिशा
2005 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और तब के भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (दिवंगत) के बीच हुआ न्यूक्लियर डील रिश्तों में ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। 2008 में यह समझौता औपचारिक रूप से लागू हुआ और दशकों की 'दूरी' खत्म होकर रिश्ता 'संरचनात्मक सहयोग' में बदल गया। इसके बाद रक्षा साझेदारी ने गति पकड़ी और समुद्री सहयोग इस साझेदारी का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा — ऐसा स्तंभ जो राजनीतिक बदलावों के बावजूद कायम रहा।
क्वाड और इंडो-पैसिफिक में साझा दृष्टिकोण
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बना क्वाड समूह किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन की तरह नहीं है, लेकिन इसका मकसद चीन की समुद्री आक्रामकता को संतुलित करना और इंडो-पैसिफिक में नियम-आधारित व्यवस्था (Rules-Based Order) को बनाए रखना है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त देती है। भारतीय नौसेना पर्शियन गल्फ से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य तक के समुद्री मार्गों पर प्रभावी निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है।
भरोसे की नई लहर
भारत-अमेरिका की रक्षा साझेदारी, खासकर नौसैनिक सहयोग, आज इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति-संतुलन का प्रमुख आधार बन चुकी है। दोनों देश मिलकर न केवल समुद्री दबाव को रोकने और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, बल्कि एक खुले और स्वतंत्र समुद्री क्षेत्र के समर्थक भी हैं। हाल में रूसी तेल व्यापार और टैरिफ विवाद से रिश्तों में कुछ खटास आई है, लेकिन दीर्घकालिक रणनीतिक हित इस साझेदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे।
(लेखक सी. उदय भास्कर (सेवानिवृत्त कमोडोर, नौसेना विश्लेषक) 37 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा दे चुके हैं और वर्तमान में प्रमुख सुरक्षा विश्लेषक व स्तंभकार हैं।)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video





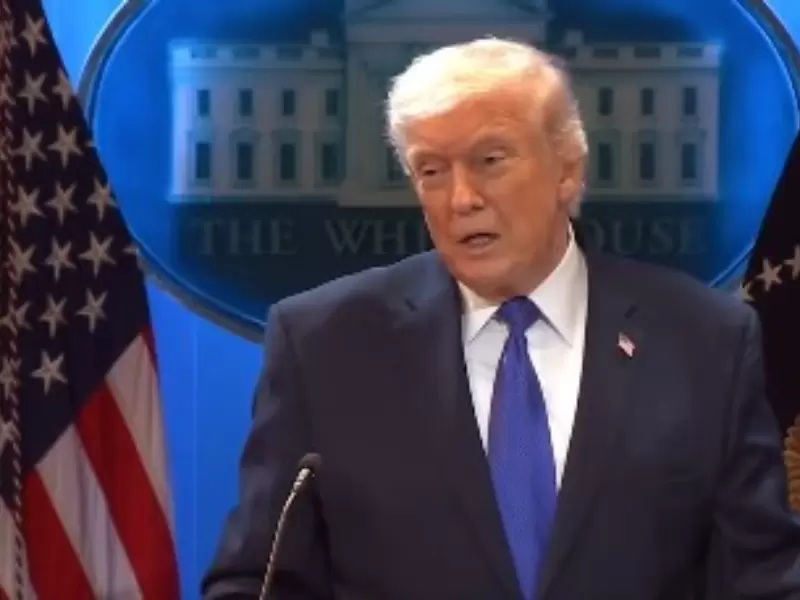

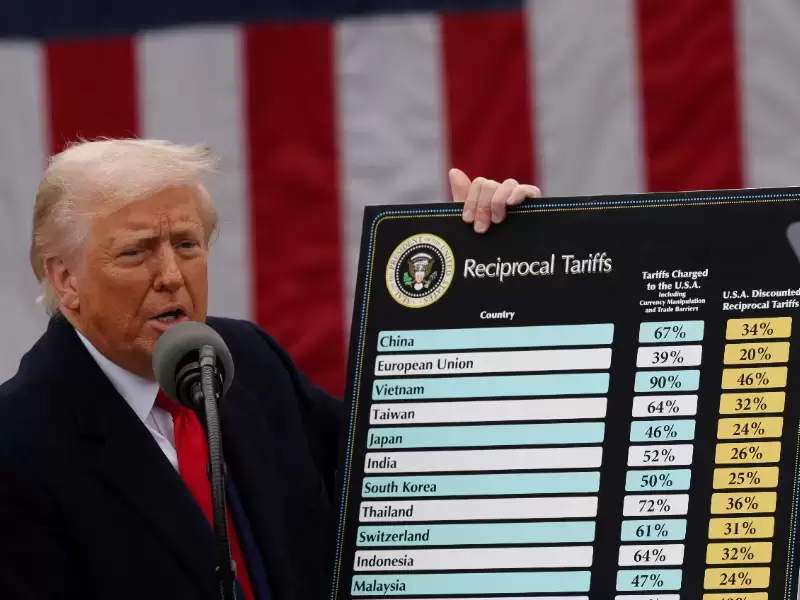








Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login