हिंदुत्व का अनावरण: जातीय-केंद्रित आख्यानों से आगे
भारत जितने आक्रमणों, वैचारिक हमलों और मिथ्याप्रस्तुतियों का सामना शायद ही किसी सभ्यता ने किया हो। इन सबके बावजूद हिंदू सभ्यता न केवल टिकी रही बल्कि फलती-फूलती रही।
 सांकेतिक तस्वीर / Pexels
सांकेतिक तस्वीर / Pexels
प्रत्येक संस्कृति अपने आप में एक दुनिया है, जिसका मूल्यांकन किसी अन्य संस्कृति के मानकों से नहीं किया जा सकता।
-फ्रांज बोआस (अमेरिकी मानवशास्त्र के जनक)
जर्मन मूल के अमेरिकी विद्वान, फ्रांज बोआस, जिन्हें व्यापक रूप से अमेरिकी मानवशास्त्र का जनक माना जाता है, ने सहानुभूति, सम्मान और वैज्ञानिक निष्पक्षता के साथ मानव विविधता को समझने की बौद्धिक नींव रखी। 1920 के दशक में, सामाजिक विकास और नस्लीय पदानुक्रम की प्रचलित धारणाओं के बीच, बोआस ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सूत्रपात किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि प्रत्येक संस्कृति को किसी अन्य संस्कृति के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उसकी अपनी दृष्टि से समझा जाना चाहिए।
बोआस से पहले, अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम ग्राहम समनर ने उस साम्राज्यवादी मानसिकता की आलोचना करने के लिए 'नृजातीय केंद्रवाद' शब्द गढ़ा था जो दूसरे समाजों का मूल्यांकन अपने मूल्यों के आधार पर करती थी। समनर की अभिजात्यवाद और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की आलोचना आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि बौद्धिक और वैचारिक नृजातीय केंद्रवाद गैर-पश्चिमी सभ्यताओं के बारे में विमर्श को प्रभावित करता रहता है।
हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद कमजोर पड़ गया लेकिन उसके मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक अवशेष अभी भी मौजूद हैं। नव-साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां अक्सर उपनिवेशीकरण के माध्यम से नहीं बल्कि पश्चिमी दर्शन को विशेषाधिकार देने वाली व्याख्याओं के ढाँचों के माध्यम से प्रकट होती हैं। यह मानसिकता वैश्विक आख्यानों को आकार देती रहती है, खासकर चिंताजनक।
भारत जितने आक्रमणों, वैचारिक हमलों और गलतबयानी का सामना शायद ही किसी सभ्यता ने किया हो। इन सबके बावजूद, हिंदू सभ्यता न केवल टिकी रही बल्कि फली-फूली भी। इसकी निरंतरता दार्शनिक बहुलवाद, आत्म-नवीकरण और सांस्कृतिक लचीलेपन पर आधारित है। फिर भी, नव-साम्राज्यवादी बौद्धिक धाराएं हिंदुत्व जैसी मूलभूत अवधारणाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करती रहती हैं और अक्सर स्वदेशी दार्शनिक ढांचों के बजाय संकीर्ण, बाह्य दृष्टिकोणों से उनकी व्याख्या करती हैं।
इसलिए, हिंदुत्व को समझने के लिए चुनिंदा व्याख्याओं और वैचारिक प्रक्षेपणों से आगे बढ़कर एक समग्र और ऐतिहासिक रूप से आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है, जिसका अर्थ सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र से हैं। ऋग्वेद (1500-1200 ईसा पूर्व) में सिंधु का सत्तर से ज्यादा बार उल्लेख मिलता है। मुख्यतः नदी के संदर्भ में। पुराने फारसी शिलालेखों में हप्त हिंदू का उल्लेख है, अरबों ने इस भूमि को अल-हिंद कहा और यूनानियों ने बाद में सिंधु का उच्चारण इंडस किया और इसके लोगों को इंडोई (भारतीय) नाम दिया।
दार्शनिक दृष्टि से, हिंदू दर्शन वैदिक सिद्धांत पर आधारित है:
एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति (ऋग्वेद 1.164.46)
सत्य एक है; ज्ञानी इसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं।
इस बहुलवादी विश्वदृष्टि ने एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जहां विविध परंपराएं, दर्शन और रीति-रिवाज सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में थे। हिंदू शब्द मूल रूप से एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता था, न कि पश्चिमी अर्थ में किसी एक धर्म को।
जब ब्रिटिश प्रशासकों को भारत की विशाल विविधता का सामना करना पड़ा तो उन्होंने इसे हिंदू धर्म के नाम से वर्गीकृत किया। जिसका पहला मुद्रित संदर्भ 1817 के आसपास मिलता है। ऐतिहासिक रूप से पापवाद, कट्टरतावाद या नस्लवाद जैसे शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय -वाद, न्यूनीकरणवादी और कभी-कभी अपमानजनक अर्थ रखता था।
महात्मा गांधी ने बड़ी ही सूक्ष्मता से कहा था:
विचार गतिशील है; जब यह ठोस हो जाता है, तो यह विचार बन जाता है; जब विचार जीवाश्म बन जाता है, तो यह वाद बन जाता है।
इस प्रकार, हिंदू धर्म शब्द उस सभ्यता का अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है जो अपने सार को संरक्षित करते हुए गतिशील रूप से विकसित होती है। इसी प्रकार, धर्म शब्द, जो हठधर्मिता और विशिष्टता को दर्शाता है, हिंदू जीवन शैली को सटीक रूप से व्यक्त नहीं करता है, जो लचीली, आत्म-चिंतनशील और धर्म में निहित है। सत्य, करुणा और जिम्मेदारी के साथ जीना और समस्त अस्तित्व का मार्गदर्शन करने वाली ब्रह्मांडीय व्यवस्था का पालन करना।
जब विदेशी भाषाओं में वैचारिक समकक्षों का अभाव होता है, तो देशी भाषाई संरचनाएं आवश्यक हो जाती हैं। संस्कृत में, प्रत्यय -त्व, अंग्रेजी के -नेस के समान, सार या अवस्था को दर्शाता है। इसी भाषाई और दार्शनिक पृष्ठभूमि में, एक प्रतिष्ठित बंगाली विद्वान, चंद्रनाथ बसु (1844-1910) ने अपनी 1892 की कृति हिंदुत्व: हिंदूर प्राकृत इतिहास (हिंदूपन: हिंदुओं का प्रामाणिक इतिहास) में हिंदुत्व (हिंदूपन) शब्द गढ़ा।
बसु ने हिंदू सभ्यता के अंतर्निहित सार, उसकी नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान, को औपनिवेशिक शब्दावली की सीमाओं से परे स्पष्ट करने का प्रयास किया। बाद में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में अपने केसरी संपादकीय 'हिंदुत्व आणि समाज सुधारना' (हिंदुत्व और सामाजिक सुधार) में, हिंदू समुदाय के भीतर ही सामाजिक सुधार पर जोर दिया।
20वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों ने भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के प्रयास किए, जिसकी परिणति 1905 में बंगाल विभाजन और उसके बाद हुए सांप्रदायिक तनावों के रूप में हुई। खिलाफत आंदोलन (1919-1924) और मोपला नरसंहार ने विभाजन को और गहरा कर दिया, जिससे भारत एक विभाजित भविष्य की ओर अग्रसर हो गया।
इस उथल-पुथल के बीच, कई स्वतंत्रता सेनानियों और विचारकों ने स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक मुक्ति के रूप में नहीं, बल्कि विचार, कर्म और आत्मा की स्वतंत्रता के रूप में देखा, जो हिंदू दर्शन में मुक्तिावस्था का सार है।
उन दूरदर्शी लोगों में विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) भी थे जो एक क्रांतिकारी, लेखक और दार्शनिक थे जिन्होंने धार्मिक विभाजन के खतरों को पहले ही भांप लिया था। 1920 के दशक की शुरुआत में जेल में रहते हुए, सावरकर ने 'एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व' की रचना की, जिसमें एक व्यापक दर्शन प्रस्तुत किया गया जो सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ता था।
भारत की 5,000 वर्षों की सभ्यतागत निरंतरता से प्रेरणा लेते हुए, सावरकर ने हिंदूत्व का वर्णन करने के लिए हिंदुत्व का प्रयोग किया—वह सभ्यतागत लोकाचार जो विजयों, उपनिवेशवाद और वैचारिक विकृतियों के बावजूद कायम रहा। जहाँ चंद्रनाथ बसु ने इस शब्द की शुरुआत की, वहीं सावरकर ने इसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों को शामिल करते हुए विस्तारित किया, जिससे हिंदुत्व को प्रतिबंधात्मक, धर्म-बद्ध शब्द हिंदू धर्म से अलग किया जा सका।
सावरकर के लिए, हिंदुत्व एक हठधर्मिता नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान थी जो भारत की विरासत और मूल्यों को साझा करने वाले सभी लोगों को एकजुट करती है। जो विचार की स्वतंत्रता, पारस्परिक सम्मान और आध्यात्मिक समावेशिता में निहित है।
अपने समृद्ध दार्शनिक आधार के बावजूद, वैश्विक विमर्श में हिंदुत्व को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के राष्ट्रवाद की धारणाओं से प्रभावित कई पश्चिमी बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता, हिंदुत्व की व्याख्या एक आक्रामक, बहिष्कारवादी या मुस्लिम-विरोधी विचारधारा के रूप में करते हैं। हालांकि, इन दावों का अनुभवजन्य आधार नहीं है और ये अक्सर वैचारिक रूप से प्रेरित आख्यानों से उत्पन्न होते हैं।
ऐसी जातीय-केंद्रित व्याख्याएं हिंदुत्व के सभ्यतागत मूल को नजरअंदाज करती हैं, जो सांस्कृतिक संश्लेषण, नैतिक बहुलवाद और आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर जोर देता है। लगातार गलत बयानी और विकृत अभियानों के बीच भी, हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग अपने सांस्कृतिक डीएनए में लंबे समय से अंतर्निहित गुणों (समावेशीपन, खुले विचारों, अहिंसा और सद्भाव की खोज) को अपनाते रहते हैं।
हिंदुत्व का सच्चा पुनरुत्थान सर्वोच्चता स्थापित करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे विश्वदृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने के बारे में है जो बयानबाज़ी से नहीं, बल्कि उदाहरण द्वारा नेतृत्व करे। यह मानवता का मार्गदर्शन उपदेशों के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यवहार द्वारा करना चाहता है। इस सार्वभौमिक आदर्श के माध्यम से:वसुधैव कुटुम्बकम यानी सारा विश्व एक परिवार है।
यह शाश्वत दर्शन हिंदू सभ्यता की चिरस्थायी भावना को प्रतिबिम्बित करता है। एक ऐसी सभ्यता जो प्रभुत्व स्थापित करने की नहीं, बल्कि एकजुट करने की आकांक्षा रखती है; धर्मांतरण की नहीं, बल्कि जोड़ने की; दुनिया को सांस्कृतिक सापेक्षवाद से देखने की नहीं, बल्कि इसे ईशावास्योपनिषद के अनुसार देखने की आकांक्षा रखती है, ईशा वश्यम् इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत (यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरीय उपस्थिति से परिपूर्ण है); और इसलिए, विभाजन की नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और साझा अस्तित्व के अभ्यास के माध्यम से मानवता का उत्थान करने की आकांक्षा रखती है।
लेखक पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति समर्पित हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय और अमेरिकी समुदायों में विभिन्न सामाजिक कार्य गतिविधियों में गहराई से शामिल हैं।
(इस लेख में व्यक्त विचार और राय लेखक के अपने हैं और जरूरी नहीं कि वे न्यू इंडिया अब्रॉड की आधिकारिक नीति या स्थिति को प्रतिबिंबित करें)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video




 डी. विट्ठल
डी. विट्ठल
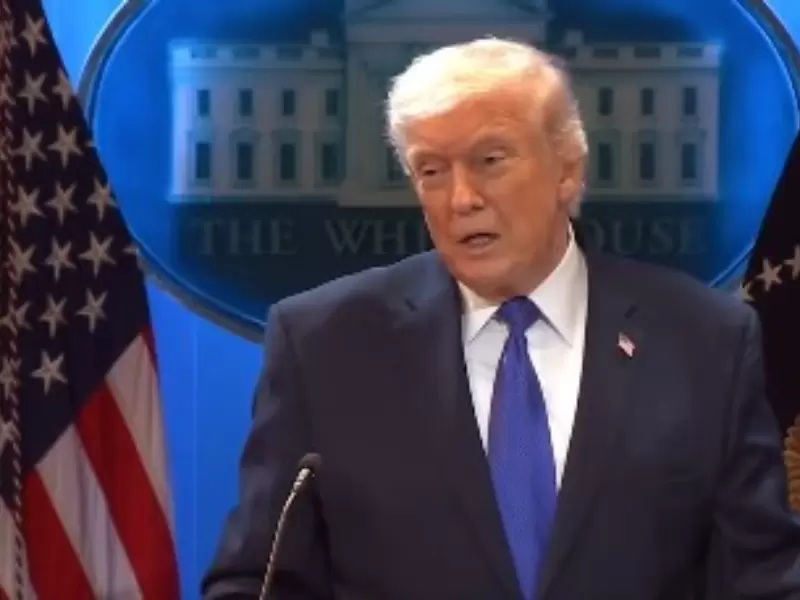

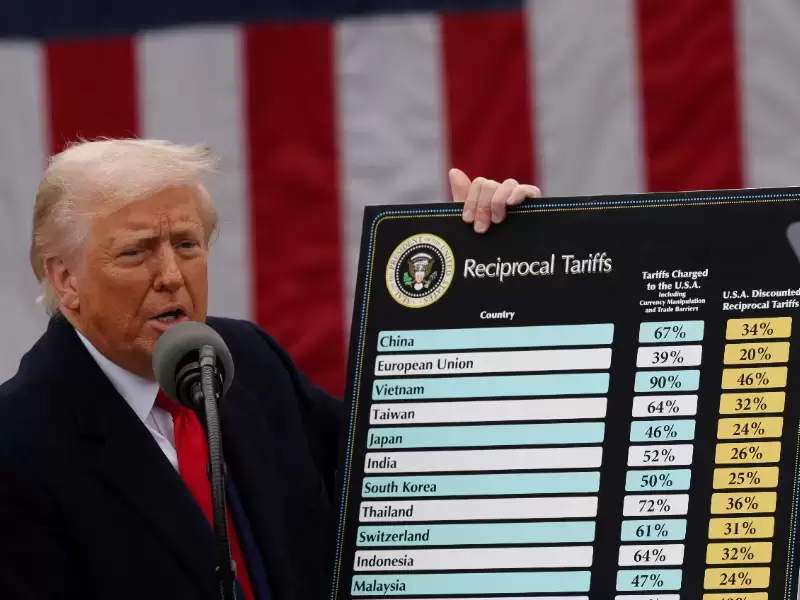








Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login