'बिहार तेज दौड़ रहा है, पर वहीं का वहीं खड़ा है'
हतर कानून-व्यवस्था, सड़कों और शासन सुधारों ने नीतीश को सुशासन बाबू बना दिया। लेकिन 20 साल बाद बिहार की कहानी परिवर्तन नहीं बल्कि पकड़-धकड़ जैसी लगती है। राज्य बदला जरूर है, पर काफी नहीं।
 (बाएं से) नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव / Wikimedia commons and Tejashwi Yadav via Facebook
(बाएं से) नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव / Wikimedia commons and Tejashwi Yadav via Facebook
बिहार चुनाव में चाहे सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति इस कड़वी सच्चाई से जरूर रूबरू होगा। राजनीतिक नेताओं द्वारा गिनाई जाने वाली उपलब्धियों दो अंकों की जीडीपी वृद्धि, रिकॉर्ड हाइवे निर्माण, ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था का सपना के पीछे यह ऐसा राज्य है जो अब भी गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की बुनियादी लड़ाई लड़ रहा है।
कागजों पर भले ही बिहार ने बीमारू राज्य का टैग उतार दिया हो लेकिन ज़मीन पर हकीकत अब भी वैसी ही है। राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिर भी यहां के लोग सबसे गरीबों में गिने जाते हैं। सड़कों, बिजलीघरों और हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है लेकिन काम करने वाले अस्पताल, टिके रहने वाले स्कूल और पर्याप्त वेतन देने वाली नौकरियां घटती जा रही हैं।
यही वह विरोधाभास है जिससे अगली कोई भी सरकार बचेगी नहीं। बिहार तेज दौड़ रहा है, पर वहीं का वहीं खड़ा है।
विकास का कठिन गणित
वित्त वर्ष 2025–26 तक बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 10.97 लाख करोड़ रुपये (लगभग 130 अरब डॉलर) तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले दस वर्षों में यह औसतन 11.4% वार्षिक दर से बढ़ा है यानी आंकड़ों में बिहार भारत के शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्यों में गिना जाता है। लेकिन जब इसे 12.7 करोड़ लोगों पर बांटा जाता है, तो तस्वीर बदल जाती है।
राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹59,637 (लगभग $720) है जो भारत के औसत का केवल एक-तिहाई है और पिछले दशक में इसमें कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ।
आर्थिक वृद्धि भी असंतुलित है
- सेवाक्षेत्र (services) का हिस्सा 58.6%,
- उद्योग (industry) का 21.5%,
- और कृषि (agriculture) का केवल 19.9% है,
जबकि कृषि में अब भी राज्य की तीन-चौथाई आबादी काम करती है। यानि यह सर्विस-आधारित वृद्धि है जो GDP तो बढ़ाती है, लेकिन टिकाऊ नौकरियां नहीं बनाती।
सामाजिक सच्चाई: प्रगति के बीच गरीबी
बिहार का मानव विकास सूचकांक (HDI) 0.609 है जो देश के सबसे निचले राज्यों में आता है। साक्षरता दर 61.8% है, जो राष्ट्रीय औसत से 11 प्रतिशत अंक कम है। हर तीन में से एक बच्चा कुपोषित है और चार में से एक बच्चा सेकेंडरी स्कूल पूरा करने से पहले पढ़ाई छोड़ देता है।
स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद कमजोर है। एक सरकारी डॉक्टर के हिस्से में लगभग 20,000 मरीज आते हैं। महिला श्रम भागीदारी दर 22.4% है जो राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है। महिलाओं और गरीबों के लिए बिहार की आर्थिक बूम अब भी एक दूर की गूंज है।
असमानता भी गहरी हो चुकी है। पटना की प्रति व्यक्ति आय 1.14 लाख रुपये है जबकि शिवहर की मात्र 18,980 रुपये है। राजधानी और गांव के बीच यह छह गुना का अंतर है। नया बिहार दरअसल दो बिहारों में बंटा है।
एक शहरी, महत्वाकांक्षी और कनेक्टेड और दूसरा ग्रामीण, कृषि-आश्रित और गरीबी के चक्र में फंसा हुआ।
अतीत की परछाईं
बिहार की मौजूदा स्थिति उसके इतिहास से अलग नहीं की जा सकती। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में राज्य आर्थिक जड़ता और प्रशासनिक पतन से गुजरा था। 1990-91 में भारत की GDP में बिहार की हिस्सेदारी 4.5% थी जो 2000 के शुरुआती वर्षों तक घटकर 2.8% रह गई। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत के 45% से गिरकर 25% पर आ गई।
जंगलराज के सालों ने बिहार को कमजोर संस्थान, खोखली नौकरशाही और डरा हुआ निवेश माहौल दिया। 2000 में झारखंड अलग हो गया जिससे बिहार की खनिज संपदा चली गई और वह लगभग पूरी तरह कृषि व प्रवासी मजदूरी पर निर्भर रह गया।
2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तब राज्य का GSDP मात्र 47,591 करोड़ रुपये था और प्रति व्यक्ति आय केवल 3,524 रुपये थी। 2001 से 2005 के बीच बिहार की वृद्धि दर औसतन 2.9% थी यानी आबादी वृद्धि से भी कम।
कमजोर बेस के कारण 2005 के बाद की वृद्धि शानदार दिखी। 2005 से 2011 के बीच औसत वृद्धि दर 11% रही, और 2006-07 में यह 17.7% तक पहुंच गई। बेहतर कानून-व्यवस्था, सड़कों और शासन सुधारों ने नीतीश को सुशासन बाबू बना दिया। लेकिन 20 साल बाद बिहार की कहानी परिवर्तन नहीं बल्कि पकड़-धकड़ जैसी लगती है। राज्य बदला जरूर है, पर काफी नहीं।
कमजोर वित्तीय रीढ़
बिहार की वित्तीय स्थिति एक और सच्चाई दिखाती है। राज्य केंद्र पर निर्भर है। करीब 75% राजस्व केंद्र सरकार से आता है वित्त आयोग के अनुदान और टैक्स डिवॉल्यूशन के जरिए। राज्य का अपना टैक्स राजस्व 59,520 करोड़ रुपये है जोकि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी जरूरी मदों के लिए भी पर्याप्त नहीं है।
सिर्फ ब्याज भुगतान 1999 के 3 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021 में 23,838 करोड़ रुपये हो गया। ऋण-से-GSDP अनुपात लगभग 40% है जो भारत में सबसे ऊंचों में से एक है।
NCAER की 2025 रिपोर्ट चेतावनी देती है कि बिहार का कर्ज स्थायित्व (debt sustainability) कमजोर है, और ब्याज का बोझ सामाजिक खर्च को दबा रहा है। यानि बिहार कर्ज लेकर आगे नहीं बढ़ रहा सिर्फ तैर रहा है।
बुनियादी ढांचे पर खर्च ने दृश्य बदलाव तो दिया है, लेकिन Gross Fixed Capital Formation (GDP में निवेश का हिस्सा) सिर्फ 4.7% है जो देश में सबसे कम है। राज्य की अर्थव्यवस्था उत्पादन नहीं, खपत पर चल रही है जो लंबे समय में अस्थिर मॉडल है।
इंफ्रास्ट्रक्चर का भ्रम
सड़क और बिजली के मोर्चे पर बिहार ने वाकई बड़ी छलांग लगाई है। 2005 में जहां ग्रामीण पक्की सड़कें 835 किलोमीटर थीं, 2025 में यह बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई हैं। राज्य में 15,987 करोड़ रुपये के 57 रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पटना मेट्रो (3,402 करोड़) बन रही है और 7,895 मेगावाट की बिजली क्षमता स्थापित हो चुकी है। लेकिन इस चमक के पीछे संस्थागत गिरावट छिपी है। सार्वजनिक निवेश की दिशा गलत होती है, भ्रष्टाचार कुशलता को खा जाता है। डिजिटल सुधारों के बावजूद बिहार अब भी Ease of Doing Business में निचले पायदान पर है। सिर्फ सड़कों से समृद्धि नहीं आती, जब इंसान और संस्थान कमजोर हों। बिहार ने सड़कों का जाल तो बिछा दिया, लेकिन अक्सर वे सड़के वापस गरीबी की ओर ही जाती हैं।
प्रवासन का जाल
बिहार का सबसे बड़ा विरोधाभास शायद उसके प्रवासन आंकड़ों में झलकता है। करीब 1 करोड़ बिहारी मजदूर राज्य के बाहर रहते हैं। दिल्ली की इमारतें, पंजाब के खेत और खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं उन्हीं से चलती हैं। ये रेमिटेंस (प्रवासी धन) ग्रामीण खपत को जीवित रखते हैं लेकिन स्थानीय श्रम बाजार को खोखला बना देते हैं। कई जिले पूरी तरह बाहर कमाए पैसे पर टिके हैं। IMF ने चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक व्यापार तनाव और रेमिटेंस में गिरावट बढ़ी तो बिहार की खपत-आधारित अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा।
सरकारें प्रवासन को समाधान नहीं, सेफ्टी वाल्व की तरह देखने लगी हैं। राज्य की बेरोजगारी ऊंची है और 75% से ज्यादा आबादी अब भी कम उत्पादक कृषि में फंसी है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना (सितंबर 2024 तक 763 करोड़ रुपये स्वीकृत) और मनरेगा वेतन सहायता कुछ राहत देती हैं। पर ये संरचनात्मक रोजगार सृजन का विकल्प नहीं हैं।
प्रकृति और उपेक्षा - दोहरी मार
हर साल कोसी और बागमती जैसी नदियों की बाढ़ उत्तर बिहार के बड़े हिस्सों को डुबो देती है। बाढ़ नियंत्रण और पुलों पर 1,478 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद तबाही जारी है। फसलें नष्ट होती हैं, सड़कें बह जाती हैं, और हर साल हजारों लोग विस्थापित होते हैं। यह सिर्फ प्राकृतिक संकट नहीं, आर्थिक संकट भी है। कृषि जो GSDP का लगभग एक-पांचवां हिस्सा देती है, लगातार असुरक्षित बनी हुई है। जलवायु झटके गरीबी को और गहराते हैं, परिवारों को कर्ज और प्रवासन के चक्र में धकेलते हैं। उधर महंगाई वास्तविक आय को खा रही है। 2023–24 में उपभोक्ता मूल्य 5.5% बढ़े जिससे गरीब परिवारों पर सीधा असर पड़ा। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की खपत बढ़ रही है लेकिन आमदनी नहीं।
राजनीति की सुस्ती
बिहार का 2025 का चुनाव भी पहले की तरह पहचान की राजनीति पर लड़ा जा रहा है। विचारों पर नहीं, जातीय गणित पर। पार्टियां मुफ्त बिजली, जातीय सर्वे, कृषि सब्सिडी और कर्ज माफी का वादा कर रही हैं लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा कि बिहार के संरचनात्मक अवरोधों को कैसे तोड़ा जाएगा। जनकल्याण ने योजना की जगह ले ली है।
नीति निरंतरता अब आर्थिक दृष्टि नहीं, राजनीतिक गठबंधन की स्थिरता पर निर्भर है। चाहे नीतीश कुमार का विकास मॉडल हो, तेजस्वी यादव का युवा कल्याण एजेंडा या भाजपा के केंद्र समर्थित प्रोजेक्ट्स। सभी को एक ही दीवार से टकराना है राज्य की वित्तीय, संस्थागत और मानवीय सीमाएं।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 कहता है कि राज्य की वृद्धि बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील है। बाढ़ से लेकर रेमिटेंस में गिरावट और वैश्विक मंदी तक। IMF का अनुमान है कि 2025–26 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रहेगी जो बिहार के निर्यात और केंद्र से मिलने वाले फंड दोनों पर दबाव डालेगी। खतरा असफलता नहीं है स्थिरता का मुखौटा है।
आगे का रास्ता
2047 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का बिहार का सपना तभी सच होगा जब विकास समावेशी होगा। इसके लिए तीन कदम अनिवार्य हैं
- अर्थव्यवस्था में विविधता लाना यानी खपत और निर्माण से हटकर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो-प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देना चाहिए खासकर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का लाभ उठाते हुए।
- मानव पूंजी में निवेश करना यानी स्कूलों, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार, विशेषकर उन ग्रामीण जिलों में जहां ड्रॉपआउट और बीमारी आम हैं।
- राजकोषीय प्राथमिकताओं का पुनर्गठन यानी अपव्यय घटाना, ब्याज बोझ कम करना और संसाधनों को उत्पादक पूंजी निवेश की ओर मोड़ना।
बिहार की आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। उन्हें आंकड़ों से नहीं, कौशल, रोजगार और सम्मान से जीना है न कि केवल नारे और सब्सिडी से।
मतदान से परे
चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली कोई भी पार्टी संकटग्रस्त नहीं बल्कि एक मोड़ पर खड़े राज्य को पाएगी। एक ऐसा राज्य जिसने जीना तो सीख लिया है पर फलना-फूलना नहीं। बिहार की समस्या अब पिछड़ेपन की नहीं, बल्कि असंतुलन की है। समावेशन के बिना विकास सिर्फ राजनीतिक भ्रम है। बिहार भले ही पहले से तेज भाग रहा हो लेकिन जब तक वह अपने लोगों को साथ नहीं उठाता, वह उसी पुराने विरोधाभास में फंसा रहेगा। जो भी पार्टी पटना में सत्ता संभालेगी, उसे एक सबसे कठिन सच्चाई का सामना करना होगा कि बिहार का असली विपक्ष विधानसभा में नहीं, बल्कि आंकड़ों में बैठा है।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video




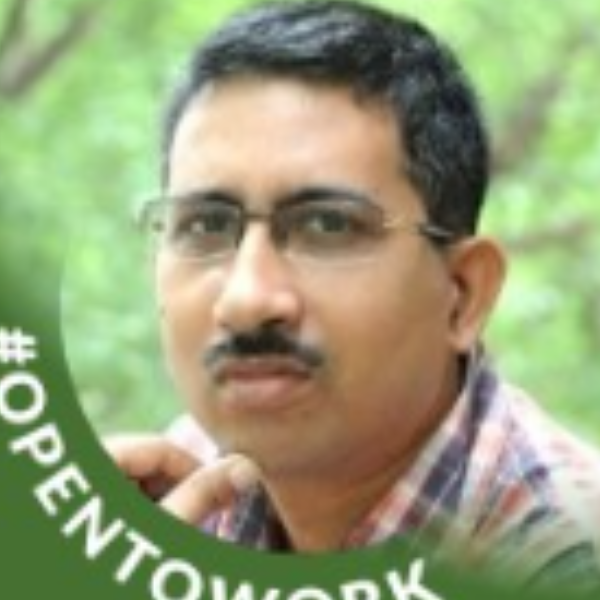 आर. सूर्यमूति
आर. सूर्यमूति









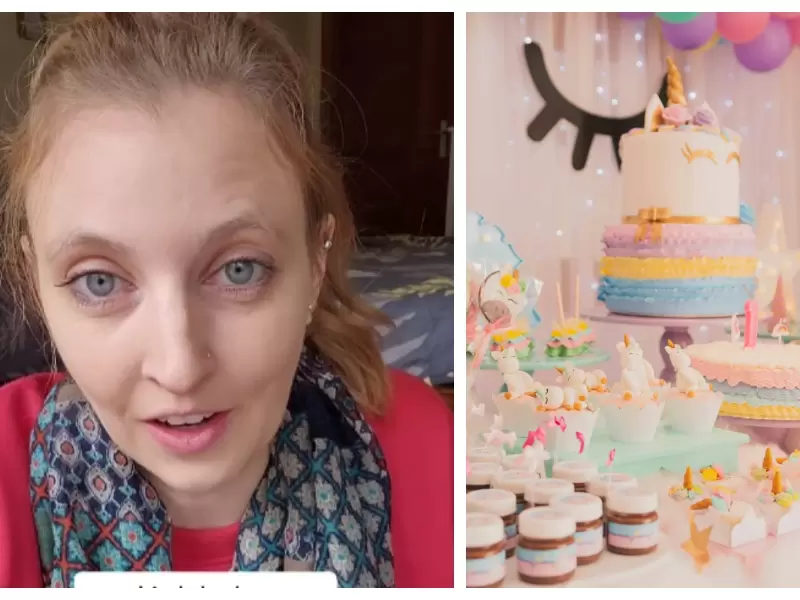



Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login