मनोज कुमार : पर्दे पर भारत... और उसके पीछे भारत कुमार
अभिनेता, लेखक, निर्देशक, संवाद लेखक और निर्माता मनोज कुमार सिर्फ भारतीय सिनेमा का हिस्सा नहीं थे; उन्होंने इसकी आत्मा को आकार देने में मदद की।
 हिंदी सिनेमा के दिग्गज अदाकार मनोज कुमार। / bollywood insider
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अदाकार मनोज कुमार। / bollywood insider
कल्पना कीजिए: सिनेमा हॉल में दर्शक स्क्रीन पर 'इंटरवल' आने से ठीक पहले जलपान के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए बस जाने को हैं। मगर वे ऐसा नहीं करते। वे मंत्रमुग्ध होकर बैठ जाते हैं क्योंकि मन्ना डे की उदास आवाज 'कसमे वादे प्यार वफा...' से ऑडिटोरियम को भर देती है। यह फिल्म थी उपकार (1967) और दर्शकों को बांधे रखने की उपलब्धि किसी और ने नहीं बल्कि लेखक मनोज कुमार ने हासिल की, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की।
संगीतकार आनंदजी विरजी शाह (कल्याणजी-आनंदजी) इसकी महानता का श्रेय कुमार की कहानी और चरित्र को देते हैं। कुमार बैकग्राउंड स्कोर में भी गहराई से शामिल थे। उन्होंने एक बार कल्याणजी-आनंदजी को एक सलाह दी थी जिसे उन्होंने अपने पूरे करियर में अपनाया कि हीरो, हीरोइन और खलनायक के लिए अलग संगीत होना चाहिए।
उन्होंने निर्देशक चंद्रा बारोट को सुझाव दिया कि वे कथा की गंभीरता को तोड़ने के लिए गीत को शामिल करें। उनके पास ऐसी कुशाग्र बुद्धि थी। जैसा कि आनंदजी ने एक बार एक साक्षात्कार में पुष्टि की थी-मनोज कुमार एक शानदार निर्देशक थे। उन्हें संगीत सुनने का शौक था। वे कहानियों को संपादित करने और लिखने में भी कुशल थे और उन्हें भारत के इतिहास का गहरा ज्ञान था।
अपने शानदार करियर के दौरान, बहुमुखी प्रतिभा वाले इस अभिनेता ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ सिनेमा में अभिनय करने को लेकर ही नहीं सोचते बल्कि इसे सिर्फ मनोरंजन करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जगाने के लिए दृढ़ विश्वास के साथ बनाते थे।
एक मिशन के साथ फिल्म निर्माण
हरि कृष्ण गिरि गोस्वामी के रूप में जन्मे मनोज कुमार ने फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के किरदार को श्रद्धांजलि देते हुए अपना स्क्रीन नाम अपनाया। उनका करियर ऐसी फिल्मों को बनाने के तरीके और अर्थ से परिभाषित हुआ जो संघर्षरत लेकिन उम्मीद से भरे भारत की आत्मा को दर्शाती हैं।
अपने निर्देशन की पहली फिल्म उपकार ने सेल्युलाइड को नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ा। कुमार ने एक सार्थक फिल्म निर्माता के रूप में अपनी जगह पक्की की। रोटी कपड़ा और मकान (1974) में उन्होंने बुनियादी मानवीय जरूरतों-भोजन, कपड़े और आश्रय-को एक ऐसी ईमानदारी के साथ चित्रित किया जो गरीबी और मोहभंग से जूझ रहे देश के साथ प्रतिध्वनित हुई।
उनकी महान कृति, क्रांति (1981) पर विचार किए बिना उनके करियर पर एक नजर अधूरी रहेगी। क्रांति यानी दिलीप कुमार और हेमा मालिनी जैसे दिग्गजों की विशेषता वाला ऐतिहासिक महाकाव्य, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अशांत दशकों तक फैला एक सिनेमाई आंदोलन था। कुमार की दृष्टि ने कई पीढ़ियों के कलाकारों को एक साथ किया और प्रतीकात्मकता किंतु व्यापक कथा प्रस्तुत की।
कुमार ने न केवल इसका निर्देशन किया, बल्कि शानदार दृश्य, ओपेरा जैसी भावनाएं, जोश से भरा बैकग्राउंड स्कोर और एक संदेश दिया कि आजादी दी नहीं जाती-उसे अर्जित किया जाता है। अपने समय की सबसे महंगी और सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक के रूप में क्रांति व्यावसायिक सफलता और राष्ट्रवादी कहानी कहने का एक दुर्लभ संयोजन था। इसने कुमार की छवि को न केवल स्क्रीन पर भारत के रूप में बल्कि एक ऐसे फिल्म निर्माता के रूप में भी स्थापित किया जो राष्ट्रीय स्तर पर भावनाओं को उभार सकता था।
उद्देश्यपूर्ण लेखनी
शहीद (1965) में कुमार द्वारा भगत सिंह का किरदार संवेदनशील और उत्साहपूर्ण था, जिसके लिए उन्हें पटकथा लेखक के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एक ऐसा पुरस्कार जिसे उन्होंने निस्वार्थ भाव से भगत सिंह के परिवार को दान कर दिया। अगर उपकार में देशभक्ति और मार्मिकता को जगह मिली, तो पूरब और पश्चिम (1970) ने पहचान, गौरव और परंपरा तथा आधुनिकता के बीच तनाव की खोज की।
देशभक्ति से परे, उन्होंने निर्माता-निर्देशक और अभिनेता के रूप में बेहद भावनात्मक शोर (1972) भी बनाई। प्रभावशाली लेखन उनके द्वारा लिखे गए संवादों तक फैला हुआ था- देशभक्ति, सामाजिक न्याय और भावनात्मक गहराई के लिए समान उत्साह से भरी पंक्तियां। तुम्हारे पास धर्म है... हमारे पास कर्म। तुम्हारे पास मंदिर है... हमारे पास इंसान। भरत पूरब और पश्चिम में कहते हैं, जो अंध धार्मिक प्रथाओं और मानवतावादी मूल्यों के बीच संघर्ष को उजागर करता है।
उनकी कलम से निकले शब्द देशभक्ति के नाटकों तक ही सीमित नहीं थे। शोर में कोमल भेद्यता हो या रोटी कपड़ा और मकान में मजदूर वर्ग का मोहभंग, जिसमें 'ये रोटी भी क्या रोटी है जो इंसान का जमीर खा जाती है?' उन्होंने अस्तित्व और गरिमा की कीमत पर सवाल उठाए। सभी विधाओं में चाहे वह ऐतिहासिक महाकाव्य हों, भावनात्मक नाटक हों या सामाजिक-राजनीतिक आख्यान-मनोज कुमार के संवाद-लेखन अपनी गहराई, उद्देश्य और बेबाक आवाज में एक समान रहे। 4 अप्रैल, 2025 को 87 वर्ष की आयु में उनका निधन एक युग का अंत था लेकिन उनकी विरासत का नहीं।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video




 बॉलीवुड इंसाइडर
बॉलीवुड इंसाइडर
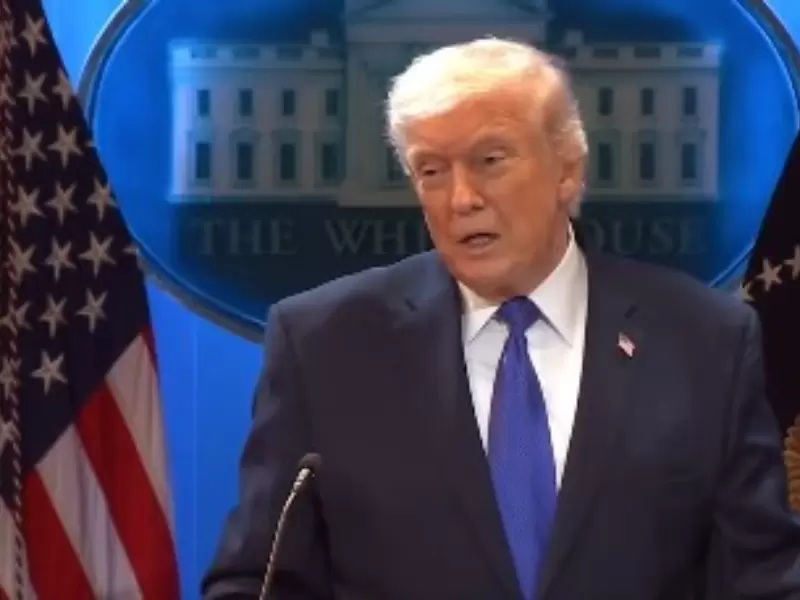

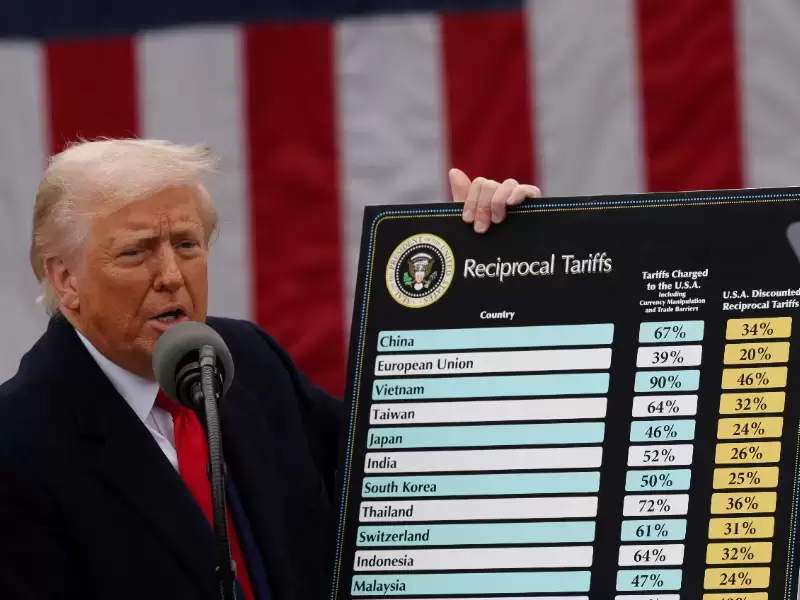








Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login